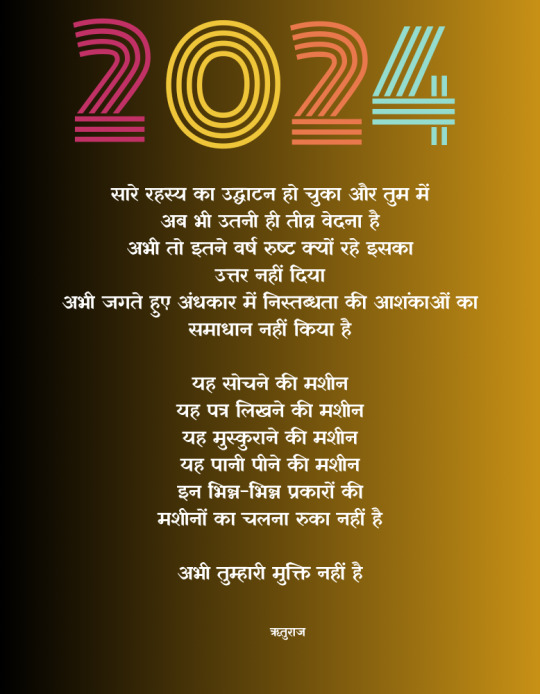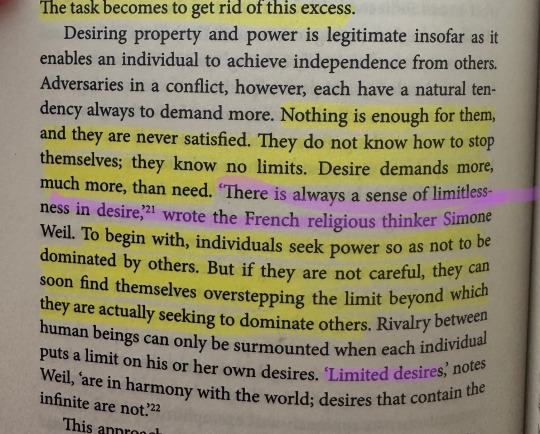Text


Dadri,
April, 2024
4 notes
·
View notes
Text
One may be very far from the ascetic view of money as a curse and yet regret that analytic therapy is almost inaccessible to poor people, both for external and internal reasons. Little can be done to remedy this. Perhaps there is truth in the widespread belief that those who are forced by necessity to a life of hard toil are less easily overtaken by neurosis. But on the other hand experience shows without a doubt that when once a poor man has produced a neurosis it is only with difficulty that he lets it be taken from him. It renders him too good a service in the struggle for existence; the secondary gain from illness which it brings him is much too important. He now claims by right of his neurosis the pity which the world has refused to his material distress, and he can now absolve himself from the obligation of combating his poverty by working.
Sigmund Freud, "On Beginning the Treatment," The Freud Reader, 370-371
15 notes
·
View notes
Text
चाहिए थोड़ा दुख
खबरें देखता रहता हूं दिन भर और
कुछ नहीं लिखता मैं
देखता हूं रील, तस्वीर और वीडियो
दूसरों का नाच गाना सोना नहाना
सब कुछ पर बेमन
सीने में जाने किसका है वजन
जो काटे नहीं कटता वक्त की तरह
गोकि मैं हूं बहुत बहुत व्यस्त और
ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है चूंकि
मैं फोन नहीं उठाता किसी का
मैं वाकई व्यस्त हूं, और जाने
किन खयालों में मस्त हूं कि अब
कुछ भी छू कर नहीं जाता
निकल लेता है ऊपर से या नीचे से
या दाएं से और बाएं से
सर्र से पर मेरी रूह को तो छोड़ दें
त्वचा तक को कष्ट नहीं होता।
ये जो वजन है
यही दुख का सहन है
वैसे कारण कम नहीं हैं दुखी होने के
दूसरी सहस्राब्दि के तीसरे दशक में, लेकिन
दुख की कमी अखरती है रोज-ब-रोज
जबकि समृद्धि इतनी भी नहीं आई
कि खा पी लें दो चार पुश्तें
या फिर कम से कम जी जाएं विशुद्ध
हरामखोर बन के ही बेटा बेटी
या अकेले मैं ही।
मैंने सिकोड़ लिया खुद को बेहद
तितली से लार्वा बनने के बाद भी
फोन आ जाते हैं दिन में दो चार
और सभी उड़ते हुए से करते हैं बात
चुनाव आ गया बॉस, क्या प्लान है
मेरा मन तो कतई म्लान है यह कह देना
हास्यास्पद बन जाने की हद तक
संन्यस्त हो जाने की उलाहना को आमंत्रित करता
बेकल आदमी का एकल गान है।
एक कल्पना है
जिसका ठोस प्रारूप कागज पर उतारना
इतना कठिन है कि महीनों हो गए
और इतना आसान, कि लगता है
एक रोज बैठूंगा और लिख दूंगा
रोज आता है वह एक रोज
और बीत जाता है रोज
अब उसकी भी तीव्रता चुक रही है
तारीख करीब आ रही है और धौंकनी
धुक धुक रही है
कि क्या 4 जून के बाद भी करते रहना होगा
वही सब चूतियापा
जिसके सहारे काट दिए दस साल
अत्यंत सुरक्षित, सुविधाजनक
बिना खोए एक क्षण भी आपा
बदले में उपजा लिए कुछ रोग जिन्हें
डॉक्टर साहब जीवनशैली जनित कहते हैं
जबकि इस बीच न जीवन ही खास रहा
न कोई शैली, सिवाय खुद को
बचाने की एक अदद थैली
आदमी से बन गए कंगारू
स्वस्थ से हो गए बीमारू
कीड़े पनपते रहे भीतर ही भीतर
बाहर चिल्लाते रहे फासीवाद और
भरता रहा मन में दुचित्तेपन का
गंदा पीला मवाद।
यार, ऐसे तो नहीं जीना था
सिवाय इस राहत के कि
जीने की भौतिक परिस्थितियां ही
गढ़ती हैं मनुष्य को
यह दलील चाहे जितना डिस्काउंट दे दे
लेकिन मन तो जानता है (न) कि
दुनिया के सामने आदमी कितनी फानता है
और घर के भीतर चादर कितनी तानता है।
अगर ये सरकार बदल भी जाए तो क्या होगा मेरा
यही सोच सोच कर हलकान हुआ जाता हूं
जबकि सभी दोस्त ठीक उलटा सोच रहे हैं
जरूरी नहीं कि दोस्त एक जैसा सोचें
बिलकुल इसी लोकतांत्रिक आस्था ने दोस्त
कम कर दिए हैं और जो बच रहे हैं
वे फोन करते हैं और मानकर चलते हैं
मैं उनके जैसी बात कहूंगा हुंकारी भरूंगा
मैं तो अब किसी को फोन नहीं करता
न बाहर जाता हूं मिलने
बहुत जिच की किसी ने तो घर
बुला लेता हूं और जानता हूं कि
दस में से दो आ जाएं तो बहुत
इस तरह कटता है मेरा क्लेश और
बच जाता है वक्त
चूंकि मैं हूं बहुत बहुत व्यस्त
बचे हुए वक्त में मैं कुछ नहीं करता
यह जानते हुए भी लगातार लोगों से बचता
फिरता हूं क्योंकि वे जब मिलते हैं तो
ऐसा लगता है कि बेहतर होता कुछ न करते
घर पर ही रहते और ऐसा
तकरीबन हर बार होता है
हर दिन बस यही संतोष
मुझे बचा ले जाता है
कि मेरा खाली समय कोई बददिमाग
पॉलिटिकली करेक्ट
बुनियादी रूप से मूर्ख और अतिमहत्वाकांक्षी
लेकिन अनिवार्यत: मुझे जानने वाला मनुष्य
नहीं खाता है।
लोगों को ना करते दुख होता है
ना नहीं करने के अपने दुख हैं
आखिर कितनों की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं
और मूर्खतापूर्ण लिप्साओं की आत्यंन्तिक रूप से
मौद्रिक परियो��नाओं में
आदमी कंसल्टेंट बन सकता है एक साथ?
आपके बगैर तो ये नहीं होगा
आपका होना तो जरूरी है
रोज दो चार लोग ऐसी बातें कह के मुझे
फुलाते रहते हैं और घंटे भर की ऊर्जा
उनके निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ जाती है
इतने में दस आदमी कांग्रेस से भाजपा में और
चार आदमी भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं
हेडलाइन बदल जाती है
किसी के यहां छापा पड़ जाता है
तो किसी को जेल हो जाती है
फिर अचानक कोई ऐसा नाम ट्रेंड करने लगता है
जिसे जानने में बची हुई ऊर्जा खप जाती है।
मुझे वाकई ये बातें जानने का शौक नहीं
ज्यादा जरूरी यह सोचना है कि अगले टाइम
क्या छौंकना है लौकी, करेला या भिंडी
और किस विधि से उन्हें बनना है
यह और भी अहम है पर संतों के कहे
ये दुनिया एक वहम है और मैं
इस वहम का अनिवार्य नागरिक हूं
और औसत लोगों से दस ग्राम ज्यादा
जागरिक हूं और यह विशिष्टता 2014 के बाद
अर्जित की हुई नहीं है क्योंकि उससे पहले भी
मैं जग रहा था जब सौ करोड़ हिंदू
सो रहा था इस देश का जो आज मुझसे
कहीं ज्यादा जाग चुका है और
मेरे जैसा आदमी बाजार से भाग चुका है
भागा हुआ आदमी घर में दुबक कर
खबरें ही देख सकता है और गाहे-बगाहे सजने वाली
महफिलों में अपने प्रासंगिक होने के सुबूत
उछाल के फेंक सकता है।
दरअसल मैं इसी की तैयारी करता हूं
इसीलिए खबरें देखता रहता हूं
पर लिखता कुछ नहीं
बस देखता हूं दूसरों का नाच गाना
सोना नहाना सब कुछ
नियमित लेकिन बेमन।
कब आ जाए परीक्षा की घड़ी
खींच लिया जाए सरेबाजार और
पूछ दिया जाए बताओ क्या है खबर
और कह सकूं बेधड़क मैं कि सरकार बहादुर
गरीबों में बांटने वाले हैं ईडी के पास आया धन।
छुपा ले जाऊं वो बात जो पता है
सारे जमाने को लेकिन कहने की है मनाही
कि एक स्वतंत्र देश का लोकतांत्रिक ढंग से
चुना गया प्रधानमंत्री कर रहा था सात साल से
धनकुबेरों से हजारों करोड़ रुपये की उगाही
खुलवाकर कुछ लाख गरीबों का खाता जनधन।
सच बोलने और प्रिय बोलने के द्वंद्व का समाधान
मैंने इस तरह किया है
बीते बरसों में जमकर झूठ को जिया है
स्वांग किया है, अभिनय किया है
जहां गाली देनी थी वहां जय-जय किया है
और सीने पर रख लिया है एक पत्थर
विशालकाय
अकेले बैठा पीटता रहता हूं छाती हाय हाय
कि कुछ तो दुख मने, एकाध कविता बने
लगे हाथ कम से कम भ्रम ही हो कि वही हैं हम
जो हुआ करते थे पहले और अकसर सोचा करते थे
किसके बाप में है दम जो साला हमको बदले।
ये तैंतालीस की उम्र का लफड़ा है या जमाने की हवा
छूछी देह ही बरामद हुई हर बार जब-जब
खुद को छुवा
हर सुबह चेहरे पर उग आती है फुंसी गोया
दुख का निशान देह पर उभर आता हो
मिटाने में जिसे आधा दिन गुजर जाता हो
दुख हो या न हो, दिखना नहीं चाहिए
ऐसी मॉडेस्टी ने हमें किसी का नहीं छोड़ा
भरता गया मवाद बढ़ता गया फोड़ा
अल्ला से मेघ पानी छाया कुछ न मांगिए
बस थोड़ा सा जेनुइन दुख जिसे हम भी
गा सकें, बजा सकें और हताशाओं के
अपने मिट्टी के गमले में सजा सकें
और उसे साक्षी मानकर आवाहन करें
प्रकृति का कि लौट आओ ओ आत्मा
कम से कम कुछ तो दो करुणा कि
स्पर्श कर सकें वे लोग, वे जगहें, वे हादसे
जिनकी खबरें देखता रहता हूं मैं
दिन भर और कुछ भी नहीं लिख पाता।
4 notes
·
View notes
Text
इस तरह
- देवी प्रसाद मिश्र
अब इसको इस तरह से करते हैं जिसे उस तरह से करते आए थे।
इस तरह से करने का मतलब होगा कि बिल्कुल नए तरह से करना।
बिल्कुल नए तरह से करने का मायने होगा कि बिल्कुल पुराने तरीके़ से नहीं करना।
लेकिन बिल्कुल नए तरीक़े से बिल्कुल पुराने तरीक़े को भुला पाना आसान नहीं
होगा। अब देखो—बिल्कुल नए तरीके़ में बिल्कुल पुराने तरीके़ के दो शब्द हैं।
तो जो बिल्कुल नया है वह बिल्कुल नया नहीं हो पाता। मतलब कि बहुत नई
भाषा में मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा वगै़रह कहाँ बदलते हैं।
बहुत नई भाषा में बहुत पुरानी चीज़ें बनी रहती हैं। इसलिए बहुत नए मनुष्य
में बहुत पुराने मनुष्य का बहुत कुछ होगा। मसलन रक्त का बहना और नंगे होकर नहाना।
11 notes
·
View notes
Text
“Imagined voices, and beloved, too, of those who died, or of those who are lost unto us like the dead. Sometimes in our dreams they speak to us; sometimes in its thought the mind will hear them. And with their sound for a moment there return sounds from the first poetry of our life– like music, in the night, far off, that fades away.”
— C.P. Cavafy, “Voices,” trans. by Daniel Mendelsohn
4 notes
·
View notes
Text
8 notes
·
View notes
Text
Things exist rooted in the flesh,
Stone, tree and flower. . . .
Space and time
Are not the mathematics that your will
Imposes, but a green calendar
Your heart observes; how else could you
Find your way home or know when to die. . . .
—R. S. Thomas, “Green Categories”
7 notes
·
View notes
Text
'What have I learned from poetry? That a political task and a political intensity can be conveyed solely through language, and that this task—although it is thoroughly commonplace—cannot be assigned by anyone, it can only be assumed by the poet in lieu of an absent people. And that nowadays no other possible politics exists, because it is solely through the poetic intensification of language that the absent people—for an instant—appears and comes to the rescue.'
--Giorgio Agamben, What I saw, heard, learned..., trans. Alta L. Price
23 notes
·
View notes
Text


बिड़हर
January, 2024
6 notes
·
View notes
Text
Into the inner world, where reason and madness mingle with hope and memory and endlessly give birth to nightmare and to dream; down into the providence of the psychiatrist and the artist, from whence spring the lunatic's fancy and the work of art. It is a dangerous region even for the artist, and his tragedy lies in the fact that in order to tap the fluid fire of inspiration, he must perpetually descend and reencounter not only the ghosts of his former selves, but all of the unconquered anguish of his living.
Ralph Ellison, "Beating that Boy" in Collected Essays, 149
33 notes
·
View notes
Text
"Amidst this operaista experience, I found myself locked in a maximum-security prison and accused of crimes of terrorism (including that of having kidnapped and killed the head of the government of a large North Atlantic country). Evidently, I had little to do with such accusations: but how should I pass the time until new clear skies? As often happens in great misfortunes, I sought refuge in the enthusiasms of adolescence and so I remembered the pantheistic passion, when I had embraced a new way of life. But now I was a communist who had gone through the class struggle which I read in terms of operaismo: how should I move in this new vital reality? What philosophical imprint, what imagination should I enact to understand the new situation? I started to read Spinoza again. What new things could he ever tell me, there, inside a prison where every year an increasing number of defeated comrades passed by an entire generation wiped out from the political and democratic scene? First of all, a "principle of hope" had to be rediscovered. And you went to search for it in Spinoza, one might ironically ask me? Yet it was precisely in Spinoza that we sought and found a principle of freedom that opened up the given being, our condition as defeated. It will not be "hope", but it looks like it. Spinoza told us that divine does not mean transcendence (but I already knew this), but rather a plural horizon of immanence, populated by infinite ways of existence, therefore with infinite capacity of singularities to build the world, not as solitary individualities but as multitudes of singular ways. My atheism then lost even the appearance of a subtle negation of transcendence: the Spinozian God was built from the bottom of ethics, in the work of singularities. Immanence was constructive freedom. I don't know if it could be called hope, it was certainly a perception of eternity. Beyond defeat, beyond the time of prison, so was the eternal being built. It did not precede us: it would follow us when we built it. But the eternal is life, and life is made up of that living work from which I, as a communist, had planned the struggle for a better future - for myself, for all the comrades with whom and for whom I had fought. Now, even though in prison, we resisted - we showed that the Communist political commitment (which our ethics was at the time) in the resistance against prison and against the destruction of our lives, prepared the revolt for the years to come. It also helped us to reorganize our knowledge. The Spinozian ethics was transformed into a communist ontology.
By contrasting Gramsci's "pessimism of reason" with the Spinozist optimism of rational imagination, by contrasting the "optimism of the will" of socialist modernism with Spinoza's "prudence" in experimenting solidarity and building common institutions."
~ Antonio Negri
Workerist Marxism: Interview with Antonio Negri by Frank Ruda and Agon Hamza
8 notes
·
View notes
Text
In this episode, Xavier Bonilla has a dialogue with Stephen Houlgate on Hegel’s Logic and his philosophy of being. They discuss the main aims of Hegel’s Logic and the use of categories, why Hegel believed Kant’s Logic is not critical enough, categories of thought and natural kinds, and separating thinking and being. They discuss Hegel and Heidegger on being, Hegel on objectivity and being presuppositionless, and pure being, becoming, and nothing. They discuss Nietzsche and Hegel on becoming, Dasein, Hegel and Frege on quantity, differential calculus, linking the Phenomenology of Spirit and Logic, and many more topics.
Stephen Houlgate is professor of philosophy at the University of Warwick. He has his PhD from the University of Cambridge and his main interest is the work of Hegel. He has published numerous books, including the most recent two volume, Hegel on Being.
0 notes